बदकिरदार
जमीर ने सायरा को तलाक देकर घर से निकाल दिया था और कई दिनों से चली आ रही खिटखिट का आज अंत हो गया था।
एक झटके से उसकी जिंदगी बदल गई थी। दुनियाबी एतबार से उसे आजाद कर दिया गया था लेकिन क्या वाकई...? वाकई वह आजाद हो पाई थी? जमीर जब उसे ब्याह कर लाया था तो लाव लश्कर के साथ गया था और आज उसे मुक्ति दी गई थी तो विदा कराने को कोई न था।
इस बीच उसने अपना सर्वस्व दे डाला था जमीर और उसके घर को... उसके परिवार के सम्मान को... उसकी परंपरागत मर्यादाओं को। अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी देह... बचा ही क्या था उसके पास? जब वह जमीर के घर आई थी तब अट्ठारह साल की खिलती हुई नवयौवना थी और आज जब उसे उस घर से मुक्ति दी गई थी, तब वह चौंतीस साल की एक औरत थी।
इस बीच अपना सुनहरा दौर अर्पण किया था उसने जमीर को... जो शायद कभी उसका हकदार न था। उसने एक सुशील बहू की हर मर्यादा निभाई थी उसने एक चरित्रवान पत्नी की हर मर्यादा निभाई थी। जैसे चाहा जमीर ने उसे रखा— कभी उसने चूं न की। एक पत्नी के तौर पर जब भी उसने अपनी टांगें फैलाईं— जमीर के लिये फैलाईं। याद नहीं उसे, कि कभी उसकी टांगे खुद के लिये भी फैली हों। कभी उस मर्दन में अपना सुख न तलाश पाई— हमेशा जमीर की तृप्ति ही सिरमौर रही।
एक के बाद एक करके तीन बच्चे जने थे उसने और उन्हें बड़ा करने में खप गई थी वह। कभी-कभी उसे लगता था कि वह औरत नहीं थी— एक फर्ज थी। बहू के रूप में एक फर्ज, पत्नी के रूप में एक फर्ज, मां के रूप में एक फर्ज। सबकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का बोझ संभाले एक मशीन— जिसके खाते में अपने लिये कुछ नहीं था।
उसे लगता था जैसे वह एक बोझ थी— एक घर से उतार कर उसे दूसरे घर में फेंक दिया गया था और अब इस घर में उम्र कट जानी थी— लेकिन यह इतना आसान थोड़े था। वह एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखती थी जहां इन रिश्तों को जोड़ना और तोड़ना बड़ा सरल करके रखा गया है— यह समझे बगैर कि इससे एक औरत की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो जाती है।
उम्र के इस पड़ाव पर, जहां तीन बच्चों में से छोटा बेटा भी दस साल का हो गया हो— उसकी जिंदगी स्थिर हो जानी चाहिये थी, लेकिन उसके समाज में स्थिरता शायद बुढ़ापे तक नहीं मिलती।
जमीर को कम उम्र की किसी बेवा से इश्क हो गया था और न सिर्फ वह अपना ज्यादातर ध्यान उसकी तरफ देता था बल्कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसी पर खर्च करने लगा था। हमेशा गूंगी गुड़िया बनी सायरा पहली बार बोलना, सवाल करना सीख पाई तो जवाब में उसे पहले डांट से शुरू होकर बाद में गालियां और फिर मार भी मिलने लगी थी।
वह चाहती थी कि शोषण के खिलाफ उसके सास-ससुर, जेठ-देवर बोलें— लेकिन वे भी तो उसी सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग थे। वह चाहती थी कि उसके पेट से पैदा तीनों बेटे उसके साथ खड़े हों, लेकिन वे भी तो भविष्य के मर्द थे।
उसके लिये खड़ा होने वाला, लड़ने वाला न यहां कोई था और न मायके में। मां बस सब्र का दामन थामे रहने की सीख देती थी और बाप मजबूर था, क्योंकि घर की व्यवस्था बेटों के जिम्मे आ चुकी थी और वह कब चाहते कि बहन किसी झगड़े का शिकार होकर वापस घर आ जाये और उनकी छाती पर मूंग दले।
एक व्यवहारिक दुनिया में— चाशनी से सराबोर, फैंसी लफ्जों से इतर, रिश्तों की हकीकत यही होती है कि वे निभाये कम और ढोये ज्यादा जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह कोई अल्लाह मियां की गाय जैसी सीधी थी कि सामने पेश होने वाले हर दुख, आघात को अपनी नियति मान कर चुपचाप बर्दाश्त करती चली जाती। सर्टिफिकेट के नाम पर भले इंटरमीडिएट तक पढ़ी थी लेकिन पढ़ने लिखने में रुचि थी तो किताबें या नेट पर काफी कुछ पढ़ती रहती थी और उसे अपना हक पता था।
भले वो खुल कर लड़ न पाती हो अपने हक के लिये लेकिन उसके मन में जब तब बगावत जरूर पैदा होती थी और यही बगावत उसे मजबूर करती थी जमीर के आगे जुबान खोलने के लिये— जिसकी परिणति कभी गाली के रूप में होती थी तो कभी मार के रूप में।
फिर आज आखिरकार वह नौबत आ ही गई थी जब जमीर ने घर में सबके सामने ही उसे तलाक दे कर, उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। या यह कहा जाये तो ज्यादा बेहतर होगा कि अपने रास्ते का कांटा हटा दिया था।
उसे बुरी तरह झटका और सदमा लगा था... वह बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी लेकिन वह घटना घट चुकी थी और उसे यह अहसास करा गई थी कि उसके समाज में, उम्र के किसी भी मोड़ पर एक औरत की जिंदगी अनिश्चित ही होती है। उसके लिये अब सुरक्षित और निश्चित भविष्य के दरवाजे बंद हो चुके थे... दिमाग में एकदम अंधेरा भर गया था।
वह इस चोट को एकदम से सह न पाई थी और फूट-फूट कर रो पड़ी थी। उसकी तकलीफ उसकी जेठानी और देवरानी ने जरूर समझी थी— आखिर वह भी उसी के जैसी अनिश्चित जिंदगी ही तो जी रही थीं लेकिन बाकियों पर शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ा था।
घर में बातें होने लगी थी कि उसके घर फोन कर दिया जाये और वह आकर उसे ले जायें लेकिन उसकी नजर में इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
आधा घंटा लगा था उसे खुद को संभालने में... इस बीच उसके आंसू खत्म हो गये थे। फिर उसने नकाब पहना और घर की देहरी छोड़ चली थी। उसे परवाह नहीं थी कि शाम हो चुकी थी— उसे परवाह नहीं थी कि क्षितिज पर काले मेघ उमड़ रहे थे और किसी भी पल बरस पड़ने को आतुर थे।
पीछे आने के लिए बेटों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई भी तो बाप की घुड़कती निगाहों ने उनके कदम रोक दिये थे।
उसकी आंखें सब देख रही थीं लेकिन उसके दिमाग में अंधेरा था— उसके भविष्य जैसा। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह कहां जायेगी— कहां रहेगी— क्या करेगी। कोई भी लक्ष्य नहीं था— बस किसी मशीन की तरह चल पड़ी थी।
उसे होश न था, वह पैदल चलते कहां की कहां पहुंच गई थी... होश तब आया जब बारिश की पहली बूंदों ने उसे छुआ। तब उसने चौंकते हुए आसपास देखा था... वह साहिली इलाके में पहुंच गई थी, जहां कम आबादी थी और खराब मौसम के चलते सड़क सुनसान हो चली थी।
उसने किसी आश्रय की तलाश में इधर-उधर निगाह दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर एक बस स्टैंड नजर आया। वह दौड़कर वहां तक पहुंची ही थी कि तेज गरज के साथ जोरदार बारिश शुरु हो गई। मिट्टी से पानी मिलते ही ऐसी तेज सोंधी महक वातावरण में फैली कि तबीयत बेचैन हो गई।
उसके सोचने की दिशा बदलने लगी।
उसने खुद का अवलोकन किया— वो थी क्या? सबकी आकांक्षाओं को, समाज की सारी मर्यादाओं को अपने तन पर काले लबादे के रूप में लपेटे एक मशीन या कोई जानवर? उसे इस लबादे से विरक्ति होने लगी।
वह झमाझम बरसते पानी को देखने लगी... कितनी बार उसकी इच्छा हुई थी ऐसे मौसम को देख कर— कि वह भी दोनों बाहें फैलाये उतर जाये इस बारिश के बीच और खुद पर समेट ले उन चीरती हुई बूंदों को। हंस के बादलों से बात करे— कड़कती बिजली को आंख दिखाये... लेकिन हमेशा उसका औरत होना उसके आड़े आया। घर में तो बाप भाइयों की घुड़कती निगाहें, ससुराल में सास-ससुर, जेठ-पति की— उसे उस की हद में रहने की चेतावनी देती निगाहें। बच्चे अभी आधे मर्द थे— यकीनन पूरे मर्द हो जाने पर उनकी निगाहें भी यही ताना मारेंगी कि तुम्हें यह शोभा देता है मां?
पर अब तो कुछ नहीं था— सब अब पीछे छूट गया था। क्या अब वह वैसी हो सकती थी जैसी चाहती थी? उसने सुनी थी चरित्रहीन औरत की व्याख्या... निस्संदेह वे सुंदर होती हैं, क्योंकि वे नैसर्गिक होती हैं, वे प्राकृतिक होती हैं, क्योंकि चरित्र तो एक थोपा हुआ बंधन है और वे मुक्त होती हैं... उन मर्यादाओं से, वर्जनाओं से... जो समाज उन पर थोपता है। वे जी लेती हैं— अपने लिये।
अब उसे आजाद कर ही दिया गया था तो क्यों वह लोगों की इच्छाओं-आकांक्षाओं का बोझ ढोये? क्यों न आगे बढ़ कर वह पल जी ले जिन पर पूरी तरह उसका वश हो... लेकिन यह काला लबादा जंजीर था। एक आजाद सायरा के अवतरण के लिये इस खोल की बंदिश से आजाद होना जरूरी था।
उसने सख्त हाथों से बटन नोच डाले और उस बंदिश को उतार फेंका।
उस खोल से एक नई— विद्रोही तेवर वाली सायरा ने अवतरण ले लिया। अब उसके लिये किसी की निगाहों का कोई मतलब नहीं था... वह मुक्त थी, सभी तरह की सामाजिक आकांक्षाओं से। वह दौड़ कर दोनों हाथ फैलाये बीच सड़क पर आ गई। बारिश ने एक झटके से उसके बदन को सराबोर कर दिया। ठंडी बूंदों ने उसकी देह को छुआ तो एक झुरझुरी सी दौड़ गई— आसपास का सब कुछ जैसे उस पानी के साथ घुल मिल कर अस्तित्व-विहीन हो गया और वह अकेली रह गई इस धरती पर— बस वह और वह बरसते बादल!
उसने पंखों की तरह हाथ फैला लिये। चेहरा आसमान की तरफ कर लिया और उस बारिश को अपने अंतर में समाहित करने लगी।
उसे याद आया कि वह मुद्दतों से नहीं हंसी थी। जोर से हंसने का तो रिवाज ही नहीं था— कहते हैं खिलखिला कर हंसने वाली औरतें बदकिरदार होती हैं... फिर इधर लगातार तनाव! रोज की खटपट और गुस्सा, अवसाद... ढंग से हंसना तो दूर मुस्कुराने तक का भी मौका उपलब्ध नहीं था।
लेकिन अब वह वक्त पीछे छूट चुका था... वह सायरा पीछे छूट चुकी थी।
वह बेसाख्ता हंसने लगी— हंसती चली गई।
बारिश के शोर में घुली उसकी हंसी अजीब लग रही थी लेकिन उसे परवाह न थी। आज वह "कोई देखेगा तो क्या सोचेगा" के दबाव, डर, आशंका, मर्यादा, वर्जना से सर्वथा मुक्त थी। वह बस हंस लेना चाहती थी। हंसते-हंसते उसकी आंखें बहने लगीं लेकिन बारिश में पानी और आंसू की पहचान मुश्किल थी।
जब खूब भीग चुकी— खूब हंस चुकी, झूम चुकी तो उसका ध्यान बस स्टैंड पर खड़े युवक की ओर गया, जिसे वह पहले महसूस ही न कर पाई थी। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था— शायद पागल समझ रहा हो।
वह लहराते हुए उसके पास पहुंची थी और पानी के छींटे उस पर उड़ाते हुए बोली थी— "पागल नहीं हूं— बस आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है उसी का मजा ले रही हूं। हैरान होकर मत देखो— वह रही वो कोख, जिससे मैं आज पैदा हुई हूं।"
उसका इशारा वहीं लावारिस पड़े नकाब की ओर था— जिसे देख कर शायद उस युवक की समझ में आधी-अधूरी बात आ गई। वह उसका हाथ पकड़ कर उसे भी खुले में खींच लाई और वह भी भीग गया। हां— वह कुछ बोला जरूर था मगर उसके शब्द सायरा का दिमाग न समझ पाया था।
उसके बदन से एक महक उठ रही थी— तीक्ष्ण सी मर्दानी गंध, जो उसे एकदम बेचैन करने लगी। फिर उसी चरित्रहीनता की वह नैसर्गिक व्याख्या उस पर प्रभावी होने लगी और वह सोचने लगी... क्या कभी उसने पहले अपने हिस्से का सुख तलाशा था? उस चरित्र को तो उसने एक उम्र दे दी थी जहाँ हर कदम पर इच्छाओं का दमन था और दमन जनित कुंठा थी... चरित्रहीन बन कर भी एक लम्हा जी लेना चाहती थी जहाँ वह एक मुक्त और नैसर्गिक स्त्री हो।
"सुन— आज तक मैंने अपनी टांगें अपने मियां की मर्जी से ही फैलाई हैं— आज अपने लिये फैलाना चाहती हूं... साथ देगा?"
उसने क्या कहा— उसके लिये वह अहम नहीं था। उसने हाथ दबा कर सहमति जता दी थी, यही उसके लिये काफी था। दोनों भीगते हुए उस तरफ दौड़ पड़े, जहां एक नई इमारत बन रही थी। उनकी उम्मीद के मुताबिक अब इस वक्त वह जगह खाली ही पड़ी थी।
एक अंधेरे कोने में उसने खुद को अर्पण कर दिया।
जिंदगी में वह पहला संसर्ग था जहां वह हर पहल खुद से कर रही थी— जहां उसे देना नहीं था, लेना था... जहां उसे कोई डर नहीं था कि उसके बारे में क्या सोचा जायेगा। आज वह हर सुख पा लेना चाहती थी जो उसने कभी सोचा हो।
युवक का कोई चेहरा नहीं था— कोई नाम नहीं था, वह बस एक विपरीत लिंगी अस्तित्व था जो उपभोग के लिये पूरी तरह समर्पित था और हर कदम पर उसे मनचाहा सहयोग कर रहा था। बाहर बारिश का संगीतमय शोर था और उस अंधेरे कोने में उन्मुक्त संगीतमय सिसकारियां!
फिर वह मुकाम भी आया कि उसके बदन में जोर की घंटियां बजने लगीं। नसों में तीव्र एंठन हुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर दबा हुआ कुछ टूट कर बह चला हो। उसका गम, उसका गुस्सा, उसकी मायूसी, उसकी फिक्र— सब कुछ जैसे उसकी नस-नस से निचुड़ कर बह निकला हो और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बेहद हल्की हो गई हो... किसी खुश्क पत्ते की तरह जो बस हवा के साथ उड़ता चला जा रहा हो— एकदम आजाद और निर्बाध।
उसने बस ऑर्गेजम के बारे में सुना भर था, पढ़ा था या कभी-कभार इत्तेफाकन अकेले ही जिया था, लेकिन जीवन में पहली बार आज उसे यह इस तरह महसूस हुआ था— वरना जमीर के साथ उसका सफर तो हमेशा अधूरा ही रहा था। मंजिल होती क्या है उसे पहले कभी अहसास तक न हो सका था।
उसका दिमाग एक आनंददाई सनसनाहट से भर गया और वह एकदम बेसुध हो गई।
थोड़ी देर बाद जब उसे सुध आई तो उसने खुद पर गौर किया... वह कच्ची जमीन पर फैली हुई थी। तन पर कपड़े की चिंदी न थी। वह उठ बैठी और कपड़े समेटने लगी.. उसे देख पास बैठे युवक ने भी अपने कपड़े समेट लिये लेकिन अब वह उसके लिये अस्तित्व-विहीन था।
उसने कपड़े निचोड़े और पहन लिये।
बाहर बारिश का दौर गुजर चुका था लेकिन वह बारिश उसे धो गई थी... उसे निखार गई थी। जो हुआ उसका कोई दुख न था— कोई पछतावा न था। एक झटके से बदल गई थी वह— अब उसके मन में न गम था, ना आक्रोश, न आंखों में भविष्य की फिक्र। होंठों पर एक गर्वीली मुस्कुराहट थी और निगाहों में वह आत्मसम्मान जो पहले कभी न महसूस कर पाई थी।
पहले बेहाली में इधर चली आई थी लेकिन अब होशो हवास में वापस लौट रही थी। थोड़ा आगे चल कर उसे एक ई-रिक्शा मिल गया और उसके सहारे वह वापस छोड़े हुए घर पहुंच गई।
उसे देख कर सब हत्प्रभ हो गये। गई थी तो कुछ और थी और आई थी तो कुछ और है... उसकी आंखों में जो तेज था— उसका सामना करने में उन्हें झुरझुरी आ गई लेकिन उसके होठों पर हंसी थी।
"क्या लेने आई है— और यह क्या हाल बना रखा है?" जमीर ने गुर्राते हुए कहा।
"क्या हाल... काली जंजीरों से बुना कपड़ा ही तो उतारा है और बाकी तो वैसे ही है। बाकी लेने क्या आई हूं का जवाब यह है कि जब गई थी तब होश में न थी अब होश में आई हूं तो याद आया कि मेरा बहुत सा सामान यहां पड़ा है, वह भी तो चाहिये न— आगे काम आना है। फिर देखो न, कपड़े भी भीग गये हैं... वह भी तो बदलने हैं।"
किसी के मुंह से बोल न फूटा।
उसने कपड़े बदले... अपने कपड़े, जेवर, दूसरा जरूरी सामान, बैग में भरकर काम खत्म किया और बच्चों को प्यार कर के आंगन में आ गई जहां सभी जड़वत् खड़े बेचैनी से बस उसे देख रहे थे— महसूस कर रहे थे।
"हे जमीर— शुक्रिया!" उसने मुस्कुराकर आंख मारते हुए कहा।
"किस बात का?" वह भड़का जरूर, पर इतना ही कहते बन पड़ा।
"मुझे आजाद करने के लिये... मुझे नयी जिंदगी देने के लिये। मुझे वह मौका देने के लिये कि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं— अपने तरीके से।" उसने हंसते हुए कहा था और वह सब ऐसे देखने लगे थे जैसे वह पागल हो गई हो।
"बहुत खुश हो आज।" जमीर ने नफरत भरे स्वर में कहा।
"हाँ रे, पैदा तो चौंतीस साल पहले हो गयी थी लेकिन आजाद आज हुई हूँ तो खुश भी न होऊं अपनी आजादी पे।" जवाब उसने मुस्कराहट के साथ ही दिया था।
"तुम्हें गुस्सा नहीं है?" ससुर ने पहली बार मुंह खोला।
"किस बात का गुस्सा करूँ— कि मुझे आजाद क्यों कर दिया, मैं तो अब बची खुची जिंदगी अहसानमंद रहूंगी कि आपके बेटे ने मुझे मौका तो दिया एक इंसान होने का... वर्ना अब तक तो मैं औरत थी।"
"तुम पागल हो गयी हो।" जमीर ने तिलमिलाते हुए कहा।
"ऊंहू, मैं आजाद हो गयी हूँ। हाँ यह आजादी तुम्हें न भायेगी, जानते हो क्यों... क्योंकि आजाद औरत एक 'मर्द' को कभी नहीं भाती, क्योंकि आजाद औरत बोलती है, क्योंकि बोलने वाली औरत एक 'मर्द' की आंख और कान में कील की तरह चुभती है।"
"तुम्हें गम नहीं है कोई।" सास ने हैरानी से पूछा।
"किस बात का? मुझे खुशी है कि इस मआशरे से निकल कर मुझे अपनी जिंदगी, अपने तरीके से जीने का मौका मिला।" उसने उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया।
"कहां जाओगी?" जेठानी ने बोझिल स्वर में पूछा।
"बाहर रिक्शा खड़ा है— पहले तो सीधे अपने घर पर ही जाऊंगी। कई रातों से ठीक से सोई नहीं हूं... आज खूब सोऊंगी। कल अपना घर भी छोड़ दूंगी। सिलाई आती है तो किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूंगी... रहने का जुगाड़ भी हो ही जायेगा। फिर कोई पसंद का मर्द मिल गया तो शायद वापस शादी भी कर लूं... वरना ऐसे भी गुजर ही जायेगी। हां खबरदार... जो इद्दत या हलाला का सोचा भी तो।"
"अम्मी।" छोटा बेटा रो पड़ा।
"मत रो बेटा, जल्दी ही भूल जायेगा मुझे... तेरी नयी मम्मी के आने के बाद। आखिर तू भी तो मर्द है न बेटा... तुझे भी आगे अपने मर्द होने का पास रखना है। चलती हूं... अल्लाह हाफिज।"
और वह चल पड़ी... पीछे सभी उसे मुंह खोले देखते रहे।
(मेरी किताब गिद्धभोज से ली हुई एक कहानी)

















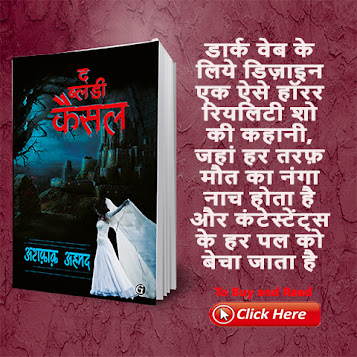



Post a Comment